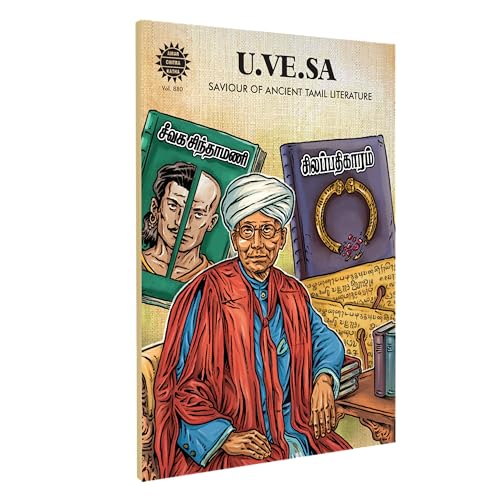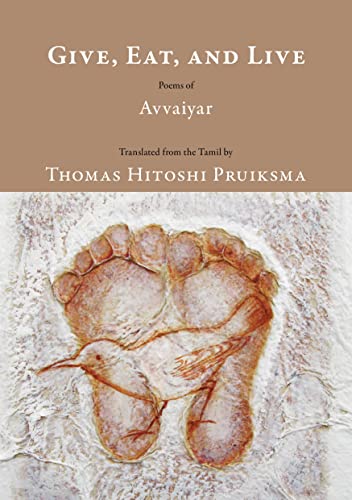पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991: समानता और ऐतिहासिक अन्याय का प्रश्न
भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जहां विभिन्न धर्म, संस्कृतियां और परंपराएं एक साथ समन्वय बनाकर चलती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 सभी नागरिकों को समानता और भेदभाव से मुक्ति का अधिकार प्रदान करते हैं, जो देश की सामाजिक और धार्मिक एकता को मजबूत करने का आधार बनते हैं। हालांकि, पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991, जो धार्मिक स्थलों की स्थिति को 15 अगस्त, 1947 के आधार पर यथास्थिति बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया था, पर यह आरोप लगता रहा है कि यह हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और आदिवासी समुदायों के साथ भेदभाव करता है। इस अधिनियम की संरचना और इसके प्रभावों ने ऐतिहासिक अन्याय, धार्मिक समानता और न्यायिक समीक्षा जैसे गंभीर मुद्दों को जन्म दिया है, जिसने इसे एक विवादास्पद कानून बना दिया है।
पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 को तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने लागू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य 15 अगस्त, 1947 को किसी भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी, उसे बनाए रखना और किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल में परिवर्तित करने पर रोक लगाना था। अधिनियम की धारा 3 और 4 स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी पूजा स्थल परिवर्तित न हो और इस संदर्भ में कोई नया मुकदमा शुरू न हो। हालांकि, अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया था। सतह पर यह कानून सामाजिक सौहार्द और धार्मिक निरपेक्षता को बढ़ावा देने वाला प्रतीत होता है, लेकिन इसकी आलोचना इस आधार पर होती है कि यह ऐतिहासिक अन्यायों को नजरअंदाज करता है और कुछ धार्मिक समुदायों के अधिकारों को सीमित करता है। आलोचकों का मानना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और आदिवासी समुदायों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंकुश लगाता है।
इस अधिनियम की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि यह मध्यकाल और औपनिवेशिक काल में हुए ऐतिहासिक अन्यायों को पूरी तरह अनदेखा करता है। अधिनियम में 15 अगस्त, 1947 को कट-ऑफ तारीख के रूप में चुना गया है, जो कई लोगों के लिए तर्कहीन और मनमाना प्रतीत होता है। मध्यकाल में, विशेष रूप से मुगल शासकों जैसे औरंगजेब के शासनकाल में, कई हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख मंदिरों और गुरुद्वारों को नष्ट कर उनके स्थान पर मस्जिदें बनाई गईं। उदाहरण के लिए, वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और मथुरा का शाही ईदगाह, जिनके बारे में ऐतिहासिक दावे हैं कि वे क्रमशः काशी विश्वनाथ मंदिर और श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के स्थान पर बनाए गए थे। इसी तरह, सिख गुरुद्वारों और आदिवासी समुदायों के पवित्र स्थलों, जैसे पवित्र वन और गुफाओं, को भी मध्यकाल और औपनिवेशिक काल में नष्ट किया गया या उन पर अतिक्रमण किया गया। औपनिवेशिक काल में, ब्रिटिश शासन के दौरान मंदिरों और गुरुद्वारों को संपत्ति के रूप में जब्त किया गया और आदिवासी पूजा स्थलों को जंगल कटाई और औपनिवेशिक नीतियों के कारण नुकसान पहुंचा। इस अधिनियम का 1947 का कट-ऑफ इन ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारने का कोई अवसर प्रदान नहीं करता, जिसके कारण हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और आदिवासी समुदाय अपने धार्मिक स्थलों को पुनः प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं।
इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम न्यायिक समीक्षा के अधिकार को भी सीमित करता है, जो भारतीय संविधान की एक मूलभूत विशेषता है। अधिनियम की धारा 4(2) किसी भी पूजा स्थल की धार्मिक स्थिति से संबंधित मुकदमों को समाप्त करती है और नए मुकदमों पर रोक लगाती है। यह प्रावधान हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदायों को अपने ऐतिहासिक पूजा स्थलों को पुनः प्राप्त करने के लिए कानूनी रास्ता अपनाने से रोकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई समुदाय यह साबित करना चाहता है कि उसका मंदिर या गुरुद्वारा मध्यकाल में नष्ट कर मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया, तो यह अधिनियम उसे अदालत में दावा करने से रोकता है। यह संविधान के अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 26 (धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार) का भी उल्लंघन करता है। आलोचकों का तर्क है कि यह कानून एक समुदाय को दूसरे पर प्राथमिकता देता है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है।
इस अधिनियम को भेदभावपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह कुछ धार्मिक समुदायों के अधिकारों को प्रतिबंधित करता है, जबकि अन्य समुदायों को उनके दावों को आगे बढ़ाने की छूट देता है। विशेष रूप से आदिवासी समुदाय, जिनके प्राकृतिक पूजा स्थल जैसे पवित्र वन और नदियां मध्यकाल और औपनिवेशिक काल में नष्ट किए गए या उन पर कब्जा किया गया, इस अधिनियम के तहत अपने सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों को पुनः स्थापित करने का कोई रास्ता नहीं पाते। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव पर रोक के सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है। इसके अलावा, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता को एक मूल सिद्धांत के रूप में अपनाता है, जिसका अर्थ है कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाए। लेकिन इस अधिनियम को आलोचकों द्वारा धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ माना जाता है, क्योंकि यह कुछ समुदायों के धार्मिक स्थलों को पुनः प्राप्त करने के अधिकार को सीमित करता है, जबकि अन्य समुदायों को इस तरह की बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता। अयोध्या मामले को इस अधिनियम से छूट देकर असमानता को और बढ़ावा दिया गया, जिसने यह सवाल उठाया कि यदि एक धार्मिक स्थल के लिए अपवाद बनाया जा सकता है, तो अन्य स्थलों के लिए क्यों नहीं?
निष्कर्ष में, पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 एक जटिल और विवादास्पद कानून है, जो सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया था, लेकिन इसने ऐतिहासिक अन्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता जैसे गंभीर सवालों को जन्म दिया है। यह अधिनियम कुछ धार्मिक समुदायों के अधिकारों को सीमित करता है और ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने का कोई रास्ता प्रदान नहीं करता। इसके कारण यह संविधान के मूल सिद्धांतों, जैसे समानता, धर्म की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा, के साथ टकराव में प्रतीत होता है। इस अधिनियम की समीक्षा और इसमें सुधार की आवश्यकता है, ताकि सभी समुदायों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों का सम्मान हो और ऐतिहासिक अन्यायों का समाधान संभव हो सके।
इस वेबसाइट को अपने बुकमार्क में जोड़ें ताकि पूजास्थल कानून के बारे में सरल भाषा में और जान सकें, जिससे आप उन प्रावधानों, उनके उद्देश्य, कार्यान्वयन के प्रभाव, संस्कृति की रक्षा में विफलता और बहुत कुछ समझ सकें। यदि आपको यह सांस्कृतिक संरक्षण की लड़ाई के लिए महत्वपूर्ण लगा तो इसे साझा करें। धन्यवाद!
Know more about laws related to temples